योग साधना (YOG SADHANA) की उपयोगिता समाधि प्राप्त करने के लिए ही नहीं, अपितु स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क तथा स्वस्थ चिंतन हेतु भी है और एक सफल, सुखद, सन्तोषप्रद तथा शान्तिमय जीवन के लिए मनुष्य को उपर्युक्त इन तीनों निधियों का स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए जो यौगिक क्रियाओं के द्वारा ही संभव है।
योग साधना के प्रकार – YOG SADHANA KE PRAKAR
शास्त्रानुसार
योग साधना (
YOG SADHANA) के आठ अंग बताए गये हैं, जिन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है। ये आठ अंग
यम,
नियम,
आसन,
प्राणायाम,
प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान तथा
समाधि है। योग साधना के इन आठ अंगों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें पांच बहिरंग एवं अन्तिम तीन अन्तरंग साधन के अन्तर्गत रखे गये हैं। दोनों साधन वर्गों को क्रमशः शारीरिक तथा मानसिक तप भी कहा जाता है।
यद्यपि
अष्टांग योग में अन्य किसी साधन की अपेक्षा न होने से “
यम” का स्थान सर्वप्रथम है, किन्तु पूर्व के बहिरंग साधनों अर्थात् शारीरिक साधनाओं में प्राणायाम का सर्वाधिक महत्व इसलिए है कि इसके अभाव में न तो शारीरिक तप में पूर्णता आती है, न ही योग के आठवें अंग समाधि को कोई आधार मिल पाता है।
क्योंकि प्राणायाम के अनुष्ठान से ही चित्त बाह्य विषयों से विरत होता है। अतः इन विषयों से इन्द्रियों के प्रत्याहरण की क्रिया भी प्राणायाम से ही स्वतः सम्पन्न हो जाती है, जिससे समाधि तक पहुॅचने का मार्ग अत्यन्त सुगम हो जाता है। योग साधना (YOG SADHANA)
 |
| Yog Sadhana |
योग साधना में यम-नियम का महत्व – YOG SADHANA ME YAM-NIYAM KA MAHATVA
योग साधना (Yog Sadhana) में यम-नियम का बड़ा महत्वा है। यम-नियम का पालन किये बिना योग साधना में शिखर तक पहुचना मुश्किल है। आइये जानते हैं योग साधना में यम-नियम का महत्वा-
यम – YAM
“यम” शब्द का अर्थ होता है निवृत्त होना। अतः हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन तथा परिग्रह आदि त्याज्य कर्मों से निवृत्त होकर इसके विपरित अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि कर्मों में प्रवृत्त होना ही योग सम्मत यम है।
अहिंसा– अहिंसा का अत्यन्त व्यापक अर्थ होता है। सामान्यतः मन, वचन तथा कर्मादि से किसी भी प्राणी को क्लेश न पहुॅचाना ही अहिंसा है। मन तथा वचन आदि से समस्त प्राणियों के प्रति दया, मैत्री तथा परोपकार आदि सद्भावों का पोषण भी अहिंसा के अन्तर्गत आता है।
कभी-कभी अहिंसा में हिंसा का भी भ्रम हो जाता है। प्राण-हरण, यद्यपि प्रबल हिंसा है, क्योंकि प्राण ही प्राणियों की सबसे प्रिय वस्तु है, किन्तु हिंसा कर्मों में मनोवृत्ति की प्रधानता होने के कारण हर प्रकार की हिंसा कर्मों को हिंसा की कोटि में नहीं रखा जा सकता, बल्कि किसी भी हिंसा के स्वरूप का निर्णय मनोवृत्ति के अनुसार करना ही न्याय संगत होता है।
उदाहरणार्थ किसी आततायी की हत्या को दोषपूर्ण हिंसा कहना युक्तिसंगत नहीं है। समूह के प्राणरक्षार्थ किसी एक के प्राण-हरण की बाध्यता को चुनौती देना औचित्यपूर्ण नहीं। रोगनिवृत्ति हेतु शल्य क्रिया, ज्ञान प्रदानार्थ प्रताड़ना तथा प्रायश्चित हेतु दण्ड आदि का विधान अहिंसा है।
शास्त्रानुसार योग साधक को अहिंसा का महाव्रत के रूप में पालन करना चाहिए किन्तु तदर्थ अहिंसा की पूर्णतः समीक्षा भी होनी चाहिए क्योंकि निरा सांसारिक होने के कारण सभी अहिंसा कर्म महाव्रत के रूप में ग्राह्य नहीं होते।
योग साधना (
YOG SADHANA)
जिस प्रकार अष्टांग योग में प्रथम सोपान होने के कारण यम का महत्व है, उसी प्रकार यमों में प्रथम स्थान प्राप्त अहिंसा का भी महत्व है। शेष सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि अन्य चारों यम भी अहिंसामूलक ही होते हैं, जिनके अनुष्ठान, अहिंसा की निर्मलता में ही अभिवृद्धि करते हैं। एक बात अवश्य ध्यान रखने योग्य है कि इनके अभाव में अहिंसा में मालिन्य आने का भय रहता है।
सत्य– किसी वस्तु को जिस रूप में नेत्रों से देखा, आगम से सुना, तर्क या अनुमान आदि से जाना हो, उस वस्तु के ज्ञान को उसी रूप में अपने मन में धारण करना या दूसरों धारण कराना सत्य कहलाता है। किन्तु अप्रिय वंचना तथा भ्रांतिपूर्ण वचन भी अपकारक तथा दुखद होने के कारण सत्य होते हुए भी असत्य है। मनु जी ने कहा है-
सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयान्नब्रूयात सत्यमप्रियम्।
अर्थात् सत्य को प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य बोलने से न बोलना अच्छा होता है क्योंकि वह वक्ता के लिए भी अश्रेयस्कर होता है।
अस्तेय– “स्तेय” शब्द का अर्थ होता है चोरी अथवा तस्करी। स्तेय शब्द में “अ” उपसर्ग लगने से बने विपरीतार्थक शब्द अस्तेय का अर्थ होता है चोरी अथवा तस्करी न करना। अर्थात् बलपूर्वक किसी के द्रव्य का हरण न करना। यही नही, अपितु अन्यायपूर्वक दूसरे के द्रव्य को स्वीकार करने की इच्छा न करना भी अस्तेय ही है।
ब्रह्मचर्य- मन, वचन कर्म द्वारा हर प्रकार से मैथुन का परित्याग ब्रह्मचर्य है। केवल संभोग न करना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है अपितु समस्त इन्द्रियों की रक्षापूर्वक उनके द्वारा भोग्य विषयों का त्याग करते हुए उपस्थ-संयम करना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य कहलाता है।
चुंकि शास्त्रानुसार वीर्य-नाश को मरण तथा वीर्य-रक्षा को जीवन कहा गया है इसलिए वीर्य-रक्षा को ही वास्तविक ब्रह्मचर्य मानना चाहिए और ब्रह्मचर्य-पालन का यही मुख्य उद्देश्य भी है। योग साधना (YOG SADHANA)
अपरिग्रह– सामान्य जीवन हेतु अपेक्षित वस्तुओं से अधिक न धारण करना अपरिग्रह कहलाता है। उपहार, दान आदि न लेना भी अपरिग्रह है क्योंकि इनको ग्रहण करने से अर्जन, रक्षण, क्षय, मोह तथा हिंसा आदि से सम्बन्धित अनेंक समस्याओं को झेलना पड़ता है जिससे हृदय-शुद्धि नहीं हो पाती है, और अपरिग्रह का मुख्य उद्देश्य तो हृदय शुद्धि ही है।
 |
| Yog Sadhana |
नियम – NIYAM
अष्टांग योग का द्वितीय सोपान “नियम” है, जिसके शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान आदि पाँच प्रकार होते हैं।
शौच– इसके बाह्य तथा आन्तरिक दो भेद होते हैं। जल, वायु, स्थान, पात्र, भोजन, वस्त्र तथा शरीर के अंगों को स्वच्छ, शुद्ध तथा पवित्र रखना, हितकर तथा परिमित आहार द्वारा शरीर को सात्विक, स्वस्थ तथा निरोग रखना बाह्य शौच है। दया, मैत्री तथा परोपकारादि की पवित्र भावनाओं द्वारा चित्त के अभिमान, ईर्ष्या-द्वेष तथा घृणा रूपी मलों का प्रक्षालन आन्तरिक शौच के अन्तर्गत आता है।
संतोष– जीवन-यापन के लिए प्राप्त आवश्यक भोग साधनों से ही सन्तुष्ट रहना तथा उससे अधिक संग्रह करने की कदापि इच्छा न करना ही सन्तोष नियम के अन्तर्गत आता है।
सन्तोष के अभाव में साधनों की बहुलता होने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
मनुस्मृति में कहा गया है- “
सन्तोष मूलं हि सुखम्” अर्थात सन्तोष ही सुख का मूल है।
योग साधना (
YOG SADHANA)
तप– शीत-उष्ण, क्षुधा-पिपासा, सुख-दुखादि सभी प्रकार के द्वन्द्वों के बीच भी सभी प्रकार की अवस्थाओं में अविचलित रहना तप है, किन्तु इस तप से शरीर में उत्पन्न हुई पीड़ा, व्याधि तथा इन्द्रिय विकार आदि के कारण यदि वह योग साधना या सामान्य जीवन कर्त्तव्य पालन के योग्य भी नहीं रहता तो इस प्रकार का तप सर्वथा त्याज्य है।
स्वाध्याय– आध्यात्मिक शास्त्रों का नियमित अध्ययन तथा प्रणव “
ऊँ“, गायत्री आदि मंत्रों को विधि-विधानपूर्वक जप स्वाध्याय नियम कहलाता है। यह जप वाचिक, उपांशु तथा मानसिक तीन प्रकार का होता है। मानसिक जप को सर्वोत्तम कहा गया है।
ईश्वर प्रणिधान– फल की इच्छा को त्याग करके सभी कर्मों का ईश्वर को समर्पण करना ईश्वर प्रणिधान नियम कहलाता है। इसी को ईश्वर में निश्चल भक्ति भी कहा गया है। जिसमें भक्त मन, वचन तथा कर्मों से प्रत्येक क्षण उस ईश्वर में समर्पित रहकर उसी की स्तुति, स्मरण तथा पूजन-आराधना में लीन रहता है।
इस प्रकार एक योगी को योग साधना (YOG SADHANA) के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उपरोक्त यम नियम आदि साधन को अपनाते हुए बहुत ही विवेकपूर्ण और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है।


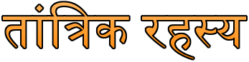



Pingback: योगा क्या है | Yoga Kya Hai » तांत्रिक रहस्य
Pingback: गुरु दीक्षा | GURU DIKSHA » तांत्रिक रहस्य
Pingback: पद्मासन (PADMASANA) : करने का तरीका और इसके लाभ » तांत्रिक रहस्य
Pingback: महिला बवासीर के 05 अचूक घरेलू उपचार » तांत्रिक रहस्य
Pingback: cialis vs mylan tadalafil
cheap generic cialis
Keren! Seperti angin sepoi-sepoi membersihkan tanah kebijaksanaan. 💨🧠 #IndosneioAnginKebijaksanaan
Keren! Seperti angin sepoi-sepoi membersihkan tanah kebijaksanaan. 💨🧠 #IndosneioAnginKebijaksanaan